ईश्वर को न जानने व न मानने वाला मनुष्य कृतघ्न और महामूर्ख होता है’
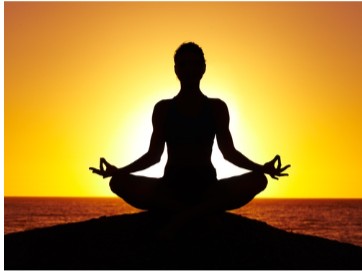
-मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून।
नुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है जिससे वह किसी भी विषय का चिन्तन कर सकता है और सत्यासत्य का निर्णय भी कर सकता है। सभी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते परन्तु जो विद्वान विद्या पढ़ते हैं, वह अपनी बुद्धि से दूसरों से अधिक जान सकते हैं तथा सत्य व असत्य को भी समझ सकते हैं। हम वर्तमान जीवन में जहां अल्पज्ञ मनुष्यों की रचनाओं को पढ़कर कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं वहीं सृष्टि में सर्वत्र व्यापक, सच्चिदानन्दस्वरूप व सर्वज्ञ ईश्वर से सृष्टि के आरम्भ में प्राप्त वेदज्ञान भी उपलब्ध है। वेदों पर हमारे प्राचीन आचार्यों, ऋषियों व विगत शताब्दी में ऋषि दयानन्द ने अनेक सैद्धान्तिक तथा इतिहास विषयक ग्रन्थों यथा ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, सत्यार्थप्रकाश आदि की रचना की हैं। हम इन ग्रन्थों का अध्ययन कर तो परमात्मा सहित सृष्टि विषयक प्रायः सभी रहस्यों को जान ही सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य अल्पज्ञ मनुष्यों की विद्या व अविद्यायुक्त बातों को पढ़कर इससे आगे की अपनी जिज्ञासायें व शंकायें दूर नहीं करते। हम देखते हैं कि सृष्टि में परमात्मा व सृष्टि विषयक ज्ञान से प्रायः सभी लोग अनभिज्ञ है। ईश्वर व आत्मा विषयक यथार्थ ज्ञान वेद व वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है।
ऋषि दयानन्द एक सच्चे जिज्ञासु थे। उन्होंने धनोपार्जन व अपने जीवन को सुखी व सम्पन्न बनाने के लिये ही ईश्वर तथा मृत्यु पर विजय पाने के उपायों सहित अन्यान्य विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था अपितु वह बुद्धि से जानने योग्य सभी विषयों को जानने के लिये अनुसंधान एवं अध्ययन में प्रवृत्त हुए थे। विद्या प्राप्त करने का उनका उद्देश्य अन्य साधारण मनुष्यों की भांति किसी प्रकार के भौतिक द्रव्यों की प्राप्ति व समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना नही था अपितु विद्या व सृष्टि के सत्य रहस्यों को जानकर उनसे होने वाले लाभों को प्राप्त करना वा जीवन से मुक्त होना था। उन्होंने इसके लिये अपूर्व त्याग एवं पुरुषार्थ किया। वह एक सच्चे योगी बने थे और अभ्यासी व अनुभवी गुरुओं से उन्होंने योगाभ्यास सीख कर ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी सफलता प्राप्त की थी। इसके साथ ही वह विद्या प्राप्ती के कार्यों में भी लगे रहे। उनकी विद्या प्राप्ती की भूख मथुरा में स्वामी विरजानन्द सरस्वती जी को आचार्य वा गुरु एवं स्वयं को शिष्यरूप में प्राप्त कर पूरी हुई थी। उनसे उन्होंने वेदांगों का अध्ययन किया था जिससे ईश्वर प्रदत्त ज्ञान वेद सहित सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का यथार्थ स्वरूप जाना व समझा जाता है। ऋषि दयानन्द महाभारत युद्ध के बाद ऐसे पहले व्यक्ति दृष्टिगोचर होते हैं जिन्होंने उपलब्ध समस्त वैदिक साहित्य का मन्थन किया था और उससे अपनी आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से सम्पन्न करने के साथ समाधि अवस्था में सभी विषयों पर प्राप्त ज्ञान की सत्यता की पुष्टि भी की थी। इस अपूर्व योग्यता को प्राप्त कर ही उन्होंने सत्य ज्ञान के प्रचार को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था।
ऋषि दयानन्द ने अपने प्रचार कार्य को वेद प्रचार का नाम दिया था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए आर्यसमाज संगठन की स्थापना कर उसका एक नियम बनाया जिसमें विधान किया कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। इससे पूर्व आर्यसमाज का तीसरा नियम यह बनाया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना व सुनना सुनाना सब आर्यों अर्थात् सत्य को जानने व मानने वाले उत्तम व श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। ऐसा इसलिये लिखा कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, वह ज्ञान आत्मा व शरीर की उन्नति करने में सर्वथा पूर्ण है और वेदज्ञान को यथार्थ रूप में प्राप्त कर ही मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं व शंकाओं का समाधान होता है। वेदाध्ययन से मनुष्य को ईश्वर व आत्मा सहित प्रकृति व सृष्टि का यथार्थ बोध हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि ईश्वर नाम की यथार्थ सत्ता इस सृष्टि व जगत में व्याप्त वा उपस्थित है। समाधि अवस्था में योगी उस परमात्मा का साक्षात्कार भी करता है। ईश्वर का साक्षात्कार करने से जीवात्मा के सभी दुःख दूर हो जाते हैं और उसे परम आनन्द की प्राप्ति होती है। ईश्वर का साक्षात्कार करना तथा परम आनन्द को प्राप्त करना ही जन्म व मरणधर्मा जीवात्मा का परम लक्ष्य होता है। इसी को प्राप्त करने के लिये हमारे पूर्वज ऋषि, मुनि, ज्ञानी व विद्वान प्रयत्न व साधना किया करते थे। ईश्वर का अस्तित्व सत्य है। वह सृष्टि में अपने गुणों से जाना जाता है। गुण, गुणी रूपी द्रव्य व सत्ता में ही रहते हैं। अतः सृष्टि की रचना व पालन का जो गुण हम सृष्टि में देख रहे हैं, उन गुणों की धारक द्रव्य सत्ता इस सृष्टि में विद्यमान सच्चिदानन्दस्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अनािद, नित्य, अजर, अमर सत्ता एक परमात्मा ही है। उसी ने इस सृष्टि को बनाया है और वही इसका पालन व धारण कर रहा है। हम ईश्वर व जीवात्मा सहित सृष्टि को इसके यथार्थ स्वरूप में वेदों सहित ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा ऋग्वेद-यजुर्वेद के भाष्यों के अध्ययन के द्वारा ही यथार्थ रूप में जान सकते हैं।
मनुष्य के पास बुद्धि है। उसका कर्तव्य है कि वह इस संसार को देखकर इसके कर्ता को जानें और उसका साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह भाग्यशाली हैं और उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर, जीवात्मा तथा सृष्टि के सत्य व यथार्थ स्वरूप को जानने की चेष्टा व प्रयत्न नहीं करते उनके जीवन व आत्मा की उन्नति न होकर परलोक वा परजन्मों अर्थात् मृत्यु के बाद मिलने वाले जन्मों में पतन ही होता है। ऋषि दयानन्द ने कहा है कि परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण अपनी शाश्वत प्रजा जीवों को उनके पूर्वजन्मों के कर्मों का सुख व दुःख रूपी फल करने तथा मोक्ष रूपी परमानन्द प्राप्त करने के लिये किया है। मोक्ष में जन्म व मरण से होने वाले सभी दुःखों का नाश हो जाता है। अतः सभी मनुष्यों को वेदाध्ययन कर ईश्वर व आत्मा सहित संसार के सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और ईश्वर की प्राप्ति की विधि सन्ध्या, ध्यान व योगाभ्यास आदि साधनों की सहायता से समाधि अवस्था को प्राप्त होकर ईश्वर का प्रत्यक्ष व साक्षात्कार करना चाहिये। ऐसा करने से मनुष्यों को ईश्वर का साक्षात्कार तो होगा ही अपितु इसके साथ परमात्मा से अक्षय सुख, मोक्षानन्द व आवागमन से मुक्ति मिलने सहित आवागमन से भी सुदीर्घकाल के लिये मुक्ति प्राप्त होगी। जो मनुष्य वेदाध्ययन सहित सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका एवं उपनिषद तथा दर्शन आदि ग्रन्थों के अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं उनको ईश्वर सहित संसार के सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान व दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि वह दृष्टि है जो मत-मतान्तर व नास्तिक लोगों को प्राप्त नहीं होती। वेदाध्ययन से प्राप्त दृष्टि से ही मनुष्यों को सत्यासत्य विशेषतः ईश्वर व आत्मा विषयक पदार्थों का यथार्थ बोध होता है। वेदों का अध्ययन करने वाला मनुष्य ईश्वर की उपासना में प्रवृत्त होता है और उससे मिलने वाले फलों धर्म सहित अर्थ, काम व मोक्ष को भी प्राप्त होता है। अतः सभी को उपासना करनी चाहिये।
उपासना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त होकर उसे उसके उपकारों के लिये स्मरण करते हुुए उसकी स्तुति, प्रार्थना व उपासना करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। सभी मनुष्य मानते भी हैं कि हम जिन मनुष्यों वा पदार्थों से कोई उपकार लेते हैं अथवा जो कोई हम पर उपकार करता है, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिये तथा उसके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना चाहिये। ईश्वर की उपासना भी उसके सृष्टि रचना करने, विभिन्न पदार्थों अग्नि, वायु, जल, अन्न, दुग्ध, फल, निवास, वस्त्र आदि हमें उपलब्ध कराने के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिये की जाती है। जो मनुष्य किसी मनुष्य का उपकार लेकर उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होता वह कृतघ्न कहलाता है। कृतघ्न होना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा देाष वा पाप है जिसका परिणाम दुःख होता है। परमात्मा के अनादि काल से हम पर अनन्त उपकार हैं जिसका ऋण चुकाने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। परमात्मा आगे भी अनन्त काल तक हमारे ऊपर उपकार करेगा। अतः हमें कृतज्ञ होकर उसकी स्तुति, प्रार्थना व उपासना करनी ही चाहिये और इनसे प्राप्त होने वाले लाभो को प्राप्त कर अपने जीवन को सुख व कल्याण से युक्त करना चाहिये। ऐसा करना युक्ति एवं तर्कसंगत भी है। इसी कारण से ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि जो मनुष्य परम उपकार करने वाले परमात्मा व उसके उपकारों को नहीं मानता वह कृतघ्न तथा महामूर्ख होता है। उनका यह कथन सर्वथा सत्य एवं यथार्थ हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते और कृतज्ञता रूप में उसकी स्तुति, प्रार्थना व उपासना नहीं करते तो निश्चय ही हम कृतघ्न सिद्ध होते हैं जिसका परिणाम हमारे लिये हानि के रूप मे ही सामने आना है। हम जन्म जन्मान्तरों में सुख व कल्याण से वंचित तथा दुःखों से युक्त रहेंगे।
हमें ईश्वर को जानना व मानना चाहिये। वेदों सहित सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों का नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिये। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना प्रतिदन प्रातः व सायं समय में अवश्य करनी चाहिये। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना व उपासना सहित वायुमण्डल की शुद्धि तथा उचित कामनाओं की सिद्धि के लिये किये जाने वाले अग्निहोत्र यज्ञ को भी नियमित करना चाहिये। जीवन में परोपकार तथा दान आदि के कार्य करने चाहिये। ऐसा करके हम ईश्वर के उपकारों के लिए उसके प्रति कृतज्ञ होने के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना से होने वाले सुख व मोक्ष आदि लाभों व आनन्द को भी प्राप्त होंगे और हम कृतघ्नता एवं महामूर्खता के पाप व दोषों से भी बचेंगे। ओ३म् शम्।
साभार :
© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.






